साहित्य सेवा के लिए यह जीवनदानी अपना गाँव-घर परिवार सब छोड़, आरा में रहता रहा और कई दशकों से वह नायब पत्रिका जनपथ निकालता रहा है. अच्छी रचनाएं मंगाना, नए लोगों से लिखवाना, उन्हें संपादित करना, ले-आउट बनाकर छापना, फिर छपी पत्रिकाओं पर पते लिख कर, उनपर डाक टिकट चिपकाना और भेजना यह सारा कुछ अपने दम पर एक योगी की तरह अनंत बाबू बिना थके बरसों तक करते रहे हैं.
वैचारिक : आरा के बहाने

हम कोलकाता में नहीं हैं जहाँ एक कवि की शवयात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं और महानगर थम जाता है. हम बंगाल में नहीं हैं जहाँ रवीन्द्र ठाकुर की तस्वीर हर घर में श्रद्धा से रखी मिलती है. हम बिहार में हैं जहाँ दस में नौ पढ़े लिखे लोग राजकमल चौधरी को नही जानते, दस में बारह महेन्दर मिसिर व भिखारी ठाकुर के बीच अगड़े पिछड़े की मंडल-मोहन रेखा खींचते हैं. हम बिहार में हैं और बिहार के कथित शहर आरा में हैं. (आरा खुद को शहर कहवाना पसंद करता है. अगर बता दिया जाए कि यार, तुम बस आबादी और आकार में थोड़ा फैले हुए, थोड़ा फूले हुए बड़े से देहात हो, शहर नहीं, तो यह शहर और इसका ‘शहरी’ बुरा मान जाता है.) तो इस कथित ‘शहर’ आरा में अगर कुछ लोगों ने सीमित साधनों से एक कथाकार/संपादक को सम्मान देने की पहल की है तो यह पहल प्रशंसनीय है. जरूरी है. लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिन्हें कहना जरूरी है.
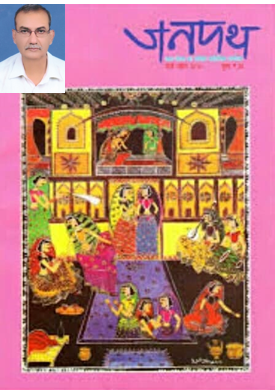
सिलसिला यूँ है कि प्रसिद्ध कथाकार और प्रतिष्ठित पत्रिका जनपथ के संपादक अनंत कुमार सिंह का सम्मान समारोह आरा के माउंट लिटरा स्कूल में रविवार को हुआ. इस कार्यक्रम के बाद से कई बातें मन मथ रही हैं. बतौर कथाकार अनंत कुमार सिंह एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, बतौर संपादक एक जरूरी हस्तक्षेप हैं. साहित्य सेवा के लिए यह जीवनदानी अपना गाँव-घर परिवार सब छोड़, आरा में रहता रहा और कई दशकों से वह नायब पत्रिका जनपथ निकालता रहा है. अच्छी रचनाएं मंगाना, नए लोगों से लिखवाना, उन्हें संपादित करना, ले-आउट बनाकर छापना, फिर छपी पत्रिकाओं पर पते लिख कर, उनपर डाक टिकट चिपकाना और भेजना यह सारा कुछ अपने दम पर एक योगी की तरह अनंत बाबू बिना थके बरसों तक करते रहे हैं.
करीब बीस साल पहले मैंने आरा रेल स्टेशन के बुक स्टाल पर पहली बार जनपथ देखा था. उसके शानदार स्तर पर मन मुग्ध हो गया. और भी सुखद आश्चर्य और गर्व हुआ जब देखा कि यह पत्रिका तो मेरे अपने शहर आरा से ही निकलती है.

आगे कुछ कहने के पहले क्षमा याचना सहित स्वीकार (कन्फेस) करता हूँ – बिना पतवार की नाव में बहते हुए मैं पत्रकारिता में तो आ गया. लेकिन साहित्य में मेरी औकात वही है जो ट्रेन के फर्स्ट क्लास में टीटी की नजर से छिपते बेटिकट यात्री की होती है. इस बेटिकट यात्री को न अपना गंतव्य मालूम, न ट्रेन का और न यह कि जो जेन्युइन लोग यहाँ हैं, वे कौन हैं, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व क्या है. तो जनपथ तो मुझे उम्दा पत्रिका लगी लेकिन उसके सर्जक अनंत कुमार सिंह कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है और उन्हें पढ़ना क्यों जरूरी है, – ये सब सवाल मेरे जेहन में कभी आए ही नहीं. वैसे भी सफेद कालर जमातों के बीच सब से कम पढ़ने वालों का कोई सर्वे हो, तो पहला स्थान पेशेवर पत्रकारों को ही मिलेगा. मैंने भी अनंत बाबू का लिखा, या और किसी का भी लिखा ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है. जब से लगने लगा कि पढ़ना जरूरी है, तब से नई समस्या यह हो गई कि अगर टीवी, फेसबुक से समय बचा भी तो कहाँ पाएं, कहाँ खोजें किताबें ? कहाँ पढ़ें पत्रिकाएँ? किनसे करें साहित्य संस्कृति पर चर्चा?

आरा में पत्रिकाओं पुस्तकों की एक भी दूकान नहीं बची है. देखते देखते ढेर सारी नई इमारतें, बाज़ार और मॉल बन गए हैं. देहाती से शहरी बन रहे आरा में गहनों कपड़ों गाड़ियों के ढेर सारे शोरूम खुल गए हैं. तनिष्क भी है और जावेद हबीब भी. लेकिन किताबों की दुकानें बंद हो गई हैं, सिनेमा हाल ठप हुए हैं, युवानीति जैसी नाटक मंडलियाँ समाप्त हो गई हैं. एक संस्कृति भवन बना है जो बंद रहता है. शायद कोई प्रेस क्लब भी है. वो भी बंद ही रहता है. बूढ़े-जवान लोगों का कहीं बैठे शतरंज खेलना पिछले जन्म की बात लगती है. और तो और बहुरूपिये तक अब नहीं आते. सब के सब राजनीति में चले गए.
समाज में आम चलन के बदलाव का एक बड़ा दौर १८५७ के बाद ग़ालिब ने देखा था. तब उन्होंने दर्ज किया था – “मुद्दत हुई है यार को मेहमां किये हुए”. लोग सोचते हैं, इस गजल में ग़ालिब महबूबा को याद कर रहे हैं. लेकिन सच ये है कि वे यार दोस्तों से मिलने जुलने का चलन मिस कर रहे हैं. स्वतंत्रता संग्राम कुचलने के बाद अंग्रेजों ने लोगों के मिलने जुलने पर रोक लगा दी थी. पारम्परिक संस्कृति में वह एक पैराडाइम शिफ्ट था. सामजिक संस्कृति में बदलाव की सुनामी का वैसा ही, कहीं ज्यादा वीभत्स, दौर हमारी पीढ़ी देख रही है. एक बार फिर लोगों ने लोगों से मिलना जुलना, चिट्ठियाँ लिखना, गाँव महल्लों में गाना बजाना ही नहीं छोड़ा, पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया है. शायद अपने चेतन अचेतन में हम सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं. शायद हमें रोबोट्स की जरूरत है ताकि मानव जाति इस पुराने ब्रह्मांड की सत्ता बिना किसी हील हुज्जत के इन नए नियंताओं को पूरी तरह सौंप सके.

कहाँ थे? कहाँ आ गए हम? – हम थे आरा में. बात कर रहे थे कि अनंत कुमार सिंह का लिखा साहित्य हम कहाँ पढ़ें, और कि जिस व्यक्ति ने आरा और इसकी साहित्यिक संपदा सींचने में कई कीमती दशक होम कर दिए, उसके सम्मान में एक इतवार को बीस जने भी क्यों जमा नहीं हुए. और जो जुटे उनमें एक भी महिला नहीं थी. एक भी छात्र नहीं था. इतने चेतना शून्य, इतने कृतघ्न इस शहर के लोग कैसे हो सकते हैं ? कुछ चूक आयोजकों से भी हुई है. आलस और अज्ञान की दीवारें बर्फ की दीवारों से ज्यादा सख्त होती हैं. उन्हें तोड़ने के लिए अतिरिक्त श्रम और बेहतर रणनीति की जरूरत है. निठल्ला बैठकबाजियों के लिए अड्डे बनाने की जरूरत है. लोगों को उनमे लाने की या खुद उनके पास जाने की जरूरत है. नए पौधों की नर्सरी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं. बैठकों का आयोजन इन्ही जगहों में किया जाए तो युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी. ऐसे ठिकाने भी बनाने होंगे जहाँ नया साहित्य और हर तरह की पत्रिकाएँ सहज उपलब्ध हो सकें. नपुंसक अप-संस्कृति की वाहक मुख्य धारा का मुकाबला गोरिल्ला पत्रिकाओं लेखकों कवियों रंगकर्मियों को करना ही होगा, अन्यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मालिक है अगले दौर का.
